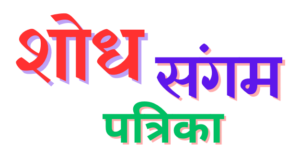हरियाणा में सनातन धर्म का सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव
Abstract
भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर से समृद्ध राष्ट्र है, जिसकी पहचान सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। सनातन धर्म कोई एक पंथ नहीं, बल्कि एक जीवनदृष्टि है, जो मानव जीवन के चार पुरुषार्थ – धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को संतुलित रूप से साधने की बात करता है। यह धर्म सहिष्णुता, करुणा, सत्य, अहिंसा और आत्मानुभूति जैसे मूल्यों पर आधारित है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस धर्म की अभिव्यक्ति भिन्न रूपों में होती आई है, और हरियाणा इस परंपरा का एक सशक्त केंद्र रहा है। हरियाणा, जो वैदिक काल में 'सरस्वती सभ्यता' का हिस्सा रहा, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी के तट पर बसी यह भूमि महाभारत के युद्धस्थल कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हरियाणा को सनातन धर्म के गहरे प्रभावों का केंद्र बनाती है। यहां की लोक संस्कृति, रीति - रिवाज, त्योहार, सामाजिक संरचना और जीवन पद्धति में सनातन परंपराओं की गूंज स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हरियाणा में सनातन धर्म का सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के दैनिक जीवन, पारिवारिक मूल्यों, आचार - विचार, तथा सामाजिक ताने - बाने में भी गहराई से समाहित है। विवाह, जन्म संस्कार, मृत्यु आदि सभी जीवन के पड़ावों पर सनातन परंपराओं की स्पष्ट झलक मिलती है। साथ ही, धार्मिक मेलों, मंदिरों, लोकगीतों, नृत्य शैलियों और लोककथाओं में भी इसकी सांस्कृतिक उपस्थिति देखी जा सकती है।
प्रेमचन्द की कहानियों में यथार्थवाद का स्वरूप
Abstract
प्रेमचन्द हिन्दी साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार हैं, जिन्होंने साहित्य को केवल कल्पना और मनोरंजन का साधन न मानकर उसे समाज परिवर्तन का औज़ार बनाया। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जब हिन्दी साहित्य आदर्शवाद और भावुकता की सीमा में बँधा हुआ था, तब प्रेमचन्द ने उसे यथार्थ की कठोर ज़मीन पर उतारा। वे हिन्दी कहानी और उपन्यास को एक नई सामाजिक चेतना, संवेदना और उद्देश्य के साथ प्रस्तुत करने वाले पहले रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। प्रेमचन्द का साहित्य मुख्यतः ग्रामीण भारत के जीवन, उसकी समस्याओं, विसंगतियों और संघर्षों का यथार्थ चित्रण करता है। उन्होंने अपने पात्रों को गाँव की मिट्टी से उठाया, जो आम जनजीवन की पीड़ा, शोषण, अभाव और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानियाँ जैसे पूस की रात, कफन, सद्गति और ईदगाह आदि में समाज के निचले तबके के जीवन का सहज और मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है।
भक्ति कालीन काव्य में सामाजिक समरसता की अवधारणा
Abstract
भक्ति कालीन काव्य भारतीय समाज में व्याप्त विषमता, जातिवाद, धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध एक सशक्त आवाज़ के रूप में उभरा। इस युग के कवियों ने भक्ति को व्यक्तिगत अनुभव के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता का माध्यम बनाया। कबीर, रविदास, मीराबाई, तुलसीदास और अन्य संत कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से सामाजिक समरसता, मानवतावाद और समता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाया। इन्होंने न केवल धार्मिक कट्टरता का विरोध किया, बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ सभी मानव बराबर हों। यह समीक्षा-पत्र भक्ति कालीन काव्य में निहित सामाजिक समरसता की अवधारणा का विश्लेषण करता है और यह दर्शाता है कि किस प्रकार भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में समन्वय और एकता की भावना को जागृत किया।