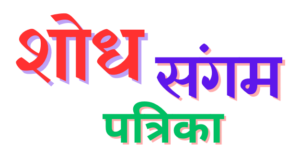| 1 |
Author(s):
विक्रान्त कौशिक, डॉ० भारत वेदालंकार.
Country:
Research Area:
संस्कृत
Page No:
1-11 |
भारतीय ज्ञान परम्परा और योग
Abstract
सम्प्रति विश्वस्य सर्वे जनाः स्वीकृतवन्तः यत् योगः जीवनस्य एकः मार्गः अस्ति यस्य दैनन्दिनस्य कार्यस्य महत्त्वपूर्णः भागः करणीयः । विश्वे सर्वेषु लेखनेषु वेदाः प्राचीनतमाः इति मन्यन्ते एतदपि सिद्धम् । ब्रह्माण्डस्य सृष्टेः अनन्तरं चतुर्णां ऋषीणां अग्निः, वायुः, आदित्यः, अङ्गिरः च ईश्वरेण एव वेदज्ञानं दत्तम् । वेदज्ञानेन सह योगविद्या अपि वर्णिता । अतः स्पष्टं भवति यत् एते ऋषयः योगाभ्यासं कृत्वा एव वैदिकमन्त्रान् दृष्टवन्तः भवेयुः । अत एव वेदे बहुषु स्थानेषु योगवर्णनं प्राप्यते । भारतीयशास्त्रेषु वेदाः सर्वशास्त्राणां आत्मा इति मन्यन्ते, स्वतः परं शास्त्रम् अपि अस्ति । वेदः ग्रन्थः यः सूर्यवत् स्वप्रकाशः अस्ति तथा च तेन सह पाठितानि सर्वाणि अपि प्रकाशयति। अध्यात्मस्य उच्चतमं शिखरं प्राप्तुं वेदानां मूलविषयः अस्ति । एतेषु सर्वेषु कार्येषु योगाभ्यासः महत्त्वपूर्णः इति मन्यते । सर्वज्ञानावस्थानां वर्णनं ब्रह्मारण्यकविभक्तशास्त्रेषु प्राप्यते, यस्मिन् पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्म इन्द्रियाणि, पञ्च वायुः, महान् शरीरं च मनसा निर्मितं भौतिकं शरीरं च वर्णनं भवति दीयते । योगसाधना याग्यकरणात् पूर्वं वेदेषु दत्तानि सर्वाणि कार्याणि करणस्य अभ्यासः इति वर्णितः अस्ति । तेन सह वेदेषु नादिप्राणयोः वर्णनमपि विद्यते, वेदेषु च यम-नियमस्य, सुगमपच्यस्य आहारस्य, शारीरिकक्रियाविधेः, मन्त्रयोङ्गस्य, लाययोगस्य च उल्लेखः अस्ति । एतैः सर्वैः प्रक्रियाभिः सह ईश्वरस्य आत्मान सह एकतायाः मुख्यसाधनत्वेन योगस्य मूलप्रयोजनम् अपि वेदेषु व्याख्यातम् अस्ति ।
| 2 |
Author(s):
भाग्य श्री ओली.
Country:
Research Area:
चित्रकला
Page No:
12-17 |
कुमाउनी जनजातीय होली का सांस्कृतिक आधार पर कलात्मक विवेचन
Abstract
कुमाऊं में होली का त्यौहार एक लोक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इसे होलिकोत्सव भी कहा जाता है। कुमाऊनी समाज में होली का त्यौहार लगभग एक या डेढ़ महीने पहले से शुरू हो जाता है। यहां का हर वर्ग इस उत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ इस त्योंहार को मनाता है। वैसे तो कुमाऊं के पहाड़ो में होली लोक उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन कुमाऊं के जनजातीय समुदाय में होली का त्यौहार कुछ भिन्न तरीके से मनाया जाता है। कुमाऊनी जनजातियों में कुछ स्थानों की होली विशेष प्रसिद्ध है। यहां जनजातियों में होली के अवसर पर गीत-संगीत के अलावा तंत्र-मंत्र, अनुष्ठानिक कला का समावेश देखने को मिलता है। यहाँ धार्मिक अनुष्ठान से लेकर ढोलक की थाप के साथ होली मनाई जाती है। वहीं होलिकोत्सव के अवसर पर कला एवं संस्कृति का अनूठा संयोजन देखने को मिलता है। ब्रज, बरसाना और मथुरा की होली ने जहां कृष्ण एवं राधा के अलौकिक प्रेम की गाथाओं को हजारों वर्षों तक जीवित कर दिया। वहीं ब्रज की गलियों से गूंजते हुए इस राधा कृष्ण के प्रेम ने पहाड़ों के प्राकृतिक सौंदर्य को एक नया स्वरूप दिया। वैसे तो उत्तराखंड के हर कोने में होली का उत्सव मनाया जाता है, परंतु कुमाऊं की जनजातीय होली ने यहां के स्थानीय लोक संस्कृति को धीरे-धीरे जीवन के अभिन्न अंग के रूप में समाहित करने में विशिष्ट योगदान है।
| 3 |
Author(s):
डॉ० मनीष ओझा.
Country:
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
18-26 |
खुसरो के साहित्य में समाज
Abstract
खुसरो का साहित्य तत्कालीन भारतीय समाज का जीवंत दस्तावेज़ है। यह वह समय है जहाँ विविध धर्मों, सम्प्रदायों, भाषाओं और संस्कृतियों का समागम हुआ। सात सौ वर्ष पहले का मध्यकालीन भारतीय समाज और उसकी संस्कृति को देखना हो तो अमीर खुसरो के साहित्य को विपुल कोष भंडार कहा जा सकता है । प्रचलित रीति-रिवाज़, बोली-बानी, वेश-भूषा, खान-पान, तीज-त्योहार, लोक विश्वास, लोक गीत-संगीत, दैनिक जीवन का रूप रंग, प्रतिदिन होने वाले क्रियाकलाप, नगर एवं ग्रामीण जीवन की झलक और ललित कलाएँ ; यानी संपूर्ण तत्कालीन भारतीय नगरीय जीवन की थाप तथा ग्रामीण जीवन की मधुर झंकार को उनके साहित्य में सुना जा सकता है ।
| 4 |
Author(s):
सुमन साहू.
Country:
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
27-32 |
समकालीन उपन्यासों में चित्रित कामकाजी महिलाएं
Abstract
समकालीन दौर में स्त्री के कामकाजी जीवन में आने वाले अनेक चुनौतियों का चित्रण हिंदी जगत के समकालीन उपन्यासकारों के उपन्यासों में देखा जा सकता है। समकालीन उपन्यासकारों में मुख्यतः मन्नू भंडारी, ममता कालिया, उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती आदि कामकाजी स्त्री के जीवन दशा को बहुत बारीकी से समझ पाई है। उनके उपन्यासों को पढ़कर हम नौकरी पेशा में कार्यरत स्त्री की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते है। यह लेखिकाएं आधुनिक महिलाओं के विचारों में आने वाले परिवर्तनों को रचना का आधार बनाती है। उनकी स्त्रियां भौतिक जगत की मार सहते हुए, आर्थिक संकटों से गुजरती नजर आती है। इनके उपन्यासों की महिलाएं कामकाजी जीवन में अनेक शारीरिक व मानसिक पीड़ा सहती हुई दिखती है। दफ्तरी जीवन में महिलाओं को परपुरुषों के हवस भरी नजरों का शिकार होना पड़ता है। कई बार यह पुरुष महिलाओं पर बलात् करने की कोशिश भी करते है । महिलाओं के साथ कार्यस्थलों पर ऐसी घटनाएं होती ही रहती है किंतु वह अपनी सूझ-बूझ व विवेक से अपनी सुरक्षा स्वयं ही करती है। समकालीन उपन्यासों में चित्रित स्त्रियां पराधीनता को अस्वीकारते हुए अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का हौसला रखती है। वह अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रखती है। स्वयं बाहरी जीवन से संघर्ष कर समाज में अपनी स्थिति मजबूत करती है। आज महिलाएं भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए पुरुष पर आश्रित नहीं रहती, बल्कि वह मेहनत कर अपनी इच्छा पूर्ति खुद करती है। कामकाजी जीवन में प्रवेश कर महिलाओं ने साबित कर दिया, कि वह अपने जीवन की स्वामिनी स्वयं है। उसे भी स्वतंत्र निर्णय लेने का तथा स्वतंत्र जीवन जीने का पूरा हक है।
| 5 |
Author(s):
मोहन महतो.
Country:
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
33-43 |
हिंदी एवं नेपाली कहानियों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक संवेदना
Abstract
धार्मिक संवेदना किसी भी व्यक्ति या समाज की आस्था, परंपरा और धार्मिक विश्वासों के प्रति उसकी भावना को दर्शाती हैl यह सहिष्णुता, सम्मान, नैतिकता और समाज में शांति स्थापित करने में सहायक होती हैl हालांकि, जब इसे कट्टरता, असहिष्णुता और सांप्रदायिकता से जोड़ दिया जाता है, तो यह सामाजिक संघर्ष का कारण भी बन सकती हैl इसलिए धार्मिक संवेदना का संतुलित और उदार दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हैl
धार्मिक संवेदना के प्रमुख पहलू हैं -आस्था और विश्वास, धार्मिक मूल्यों की रक्षा, धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द, धार्मिक आस्थाओं पर चोट का अनुभव, धर्म और समाज के बीच संबंध l साहित्य में धार्मिक संवेदना का उपयोग पौराणिक कथाओं भक्ति साहित्य नैतिक शिक्षाओं और धर्म से जुड़े सामाजिक मुद्दों के चित्रण में किया जाता है l तुलसीदास के रामचरितमानस, कबीर और सूरदास की रचनाएं धार्मिक संवेदना से भरपूर हैl आधुनिक साहित्य में प्रेमचंद से लेकर अखिलेश, संजीव, मनोज रुपाड़ा, मधु कांकरिया, अनामिका, गीतांजलि श्री जैसे साहित्यकारों ने धार्मिक संवेदना को नए दृष्टिकोण से देखा है l समाज में धार्मिक संवेदना लोगों के आचरण, रीति- रिवाज और सामूहिक जीवन को प्रभावित करती हैंl यह सामाजिक नैतिकता दान, सेवा और भाईचारे की भावना को जन्म देती है l
| 6 |
Author(s):
प्रदीप कुमार दाश ‘दीपक’, डॉ. सुरुचि मिश्रा.
Country:
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
44-51 |
प्रकृति बोध का काव्य हाइकु
Abstract
भारत एवं जापान दोनों देश के साहित्य में 'ध्यान' का बड़ा महत्व है । ध्यान भारतीय दर्शन में संसार से मुक्ति (मोक्ष/निर्वाण) की ओर ले जाने वाला एक चिंतन है। यह चेतन मन की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं की चेतना बाह्य जगत् के किसी चुने हुए स्थल-विशेष पर केंद्रित करता है। ध्यान से जीवन में दिव्यता आती है, और जब व्यक्ति इस दिव्यता का अनुभव कर लेता है, तो सारी सृष्टि उसे सुन्दर प्रतीत होने लगती है। ध्यान से व्यक्ति जीवन की समस्त बुराइयों से ऊपर उठ जाता है और इस संसार को सुंदर बनाने के कार्य में संलग्न हो जाता है । जापान में ज़ेन बौद्ध धर्म का मुख्य अभ्यास बैठ कर ध्यान करना है । सतह पर ध्यान का अभ्यास काफी आसान या सरल लग सकता है, लेकिन जिसने भी ध्यान किया है वह जानता है कि पाँच मिनट तक स्थिर रहना कितना मुश्किल हो सकता है । “ज़ेन ध्यान मुद्रा पर केंद्रित है, इसमें साँसों का अनुसरण किया जाता है । एक समय में एक साँस लेना और एक साँस छोड़ना । हर बार जब कोई विचार उठता है, तो हम विचार का अनुसरण नहीं करते हैं और साँस पर लौट आते हैं । इस तरह देखा जाए तो सचमुच साँसों से विचारों का गहरा संबंध स्थापित है । कविता' कवि के आंतरिक भाव, विचारों का उद्वेलित रूप है, इस तरह देखा जाए तो काव्य में श्वास यानी भाव व विचारों का महत्व लाजिमी है ।
| 7 |
Author(s):
धर्म वीर शर्मा, डॉ भारत वेदालंकार.
Country:
Research Area:
दर्शनशास्त्र
Page No:
52-57 |
श्रेष्ठ समाज के निर्माण में यम – नियम की भूमिका
Abstract
योग भारतीय ज्ञान परम्परा की एक ऐसी विधा है जिसे दर्शन के प्रत्येक वर्ग ने स्वीकार किया है। क्योंकि योग केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान नहीं करता अपितु व्यवहार में अंगीकार किया जाता है। बड़े-बड़े ऋषि, तपस्वी योग मार्ग का अनुसरण जीवन के परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। परंतु योग केवल ऋषि-महात्मा आदि तपस्वियों के लिए नहीं है वरन् योग सामान्य जन मानस के लिए भी उतना ही उपयोगी है। योग के द्वारा व्यक्ति का समग्र विकास होता है। योग मानव जीवन के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग का पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। योग समाज को उन्नत बनाने, शिष्ट बनाने तथा श्रेष्ठ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योगदर्शन में अष्टांग योग के अंतर्गत प्रतिपादित यम और नियम दो ऐसे आधारभूत साधन हैं जिनके पालन से व्यक्ति की आत्मिक उन्नति होती है तथा सामाजिक समरसता की भवन जागृत होती है।
| 8 |
Author(s):
अंकित भोई.
Country:
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
58-63 |
ऑपरेशन बस्तर : युद्ध और प्रेम-कथा
Abstract
इस लघु उपन्यास में देश की नक्सल राजधानी बस्तर के दुर्गम एवं नक्सल समस्या से प्रभावित क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को होने वाले कष्ट, दुविधाओं, अंतर्द्वंद्व और विपरीत परिस्थितियों में उनकी कर्त्तव्यपरायणता का वर्णन किया गया है। बेहद सरल भाषा में लिखित यह उपन्यास पाठकों के मानस पटल पर बस्तर की सांस्कृतिक महक बिखेरता है। लेखक ने बस्तर के निवासियों की नैसर्गिक सरलता, विश्वविख्यात मुर्गा-लड़ाई, नशीली सल्फी, मानव-तस्करी, शिक्षा व्यवस्था को सबल बनाने हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयास, बजरंग दल एवं रामकृष्ण मिशन की सतत सक्रियता, धर्म-परिवर्तन और माओवादी संगठन द्वारा की जाने वाली अवैध उगाही जैसे विभिन्न यथार्थ आधारित तथ्यों को परस्पर संबद्ध कर संजीदगी से बस्तर का सजीव चित्रांकन किया है। प्रेम और जंग की समानांतर कथा पर आधारित यह उपन्यास वर्ष 2020 में यश पब्लिकेशंस, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इसके लेखक भारतीय-तिब्बत सीमा पुलिसबल के पूर्व उपसेनानी श्री कमलेश कमल हैं। लेखक ने कल्पना और यथार्थ मिश्रित इस कृति को देश के युवाजनों को समर्पित किया है। प्रस्तुत रचना के माध्यम से उन्होंने सुरक्षा बल एवं नक्सली, दोनों का ही पक्ष जानने का आह्वान किया है।
| 9 |
Author(s):
महेंद्र पाल.
Country:
Research Area:
राजनीति विज्ञान
Page No:
64-73 |
एक राष्ट्र, एक चुनाव: भारत में लोकतांत्रिक सुधार की संभावनाएँ, चुनौतियाँ और नीतिगत दृष्टिकोण
Abstract
"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एक क्रांतिकारी सुधार के रूप में उभरी है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करना है। यह विचार बार-बार होने वाले चुनावों की आर्थिक, प्रशासनिक, और सामाजिक लागत को कम करने का प्रयास करता है। यह शोध पत्र इस अवधारणा के ऐतिहासिक संदर्भ, संभावित लाभ, कार्यान्वयन की चुनौतियों, और भारत की जटिल सामाजिक-राजनीतिक संरचना पर इसके प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, यह पत्र अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस प्रणाली की तुलना करता है और भारत में इसके कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक नीतिगत सुझाव प्रदान करता है। निष्कर्ष में, यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि यह अवधारणा सैद्धांतिक रूप से आकर्षक है, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए व्यापक संवैधानिक संशोधन, राजनीतिक सहमति, और तकनीकी तैयारी आवश्यक होगी।
| 10 |
Author(s):
नरेंद्र कुमार.
Country:
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
74-80 |
समकालीन कविता में राजनीतिक चेतना
Abstract
समकालीन कविता केवल सौंदर्यबोध या व्यक्तिगत अनुभूति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का गंभीर साक्ष्य बन गई है। वर्तमान समय में जब लोकतंत्र, नैतिकता, और मानवाधिकार संकट में हैं, तब समकालीन कवि सत्ता के दमन, पाखंड और विडंबना को उजागर करते हैं।
रघुवीर सहाय, धूमिल, ऋतुराज, अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, एकांत श्रीवास्तव और मदन कश्यप जैसे कवि राजनीति के अनैतिक गठजोड़, चरित्रहीन जनप्रतिनिधियों और कुर्सी की भूख में डूबी व्यवस्था पर कठोर प्रहार करते हैं।
यह कविता जनता की आवाज बनकर, उस चुप्पी को तोड़ती है जिसे सत्ता ने भय और दमन के माध्यम से स्थापित किया है। समकालीन कविता सिर्फ़ विरोध नहीं, बल्कि जन-सजगता, लोकतांत्रिक चेतना और नैतिक मूल्यबोध की पुकार है।
| 11 |
Author(s):
मोहन महतो, डॉ विनोद कुमार.
Country:
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
81-87 |
स्त्री अस्मिता और कथा-संवेदना: मनीषा कुलश्रेष्ठ और हेमन्दास राई की कहानियों का तुलनात्मक पाठ
Abstract
इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में स्त्री अस्मिता का विमर्श हिंदी और नेपाली साहित्य में एक केन्द्रीय स्थान ग्रहण करता है। यह विमर्श केवल स्त्री की शारीरिक पहचान तक सीमित न रहकर, उसके मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और जातीय संघर्षों को भी उकेरता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में हिंदी की प्रतिष्ठित कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ तथा नेपाली साहित्य के सशक्त स्वर हेमन्दास राई की कहानियों के माध्यम से स्त्री अस्मिता और कथा-संवेदना का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।इस शोध का प्रमुख उद्देश्य इन दोनों भाषाओं में स्त्री की स्थिति, संघर्ष और चेतना को समझना है—विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में। मनीषा की कहानियाँ शहरी, शिक्षित, आत्मनिर्भर स्त्री की मानसिक ऊहापोह, विरोध और आत्मसंघर्ष को दर्शाती हैं; वहीं हेमन्दास की कहानियाँ ग्रामीण, वंचित, जातीय संदर्भों में स्त्री की मौन पीड़ा और सामाजिक घुटन की अभिव्यक्ति हैं। “केयर ऑफ़ स्वात घाटी”,“बौनी होती परछाई”,“गंधर्व गाथा” कहानी संग्रह एवं “किरदार” जैसी कहानियाँ स्त्री के आत्म-संघर्ष, पहचान-निर्माण और पितृसत्ता से संघर्ष की कहानियाँ हैं। दूसरी ओर “रातो टीका”, “माछा खाने मान्छेहरू” और “अभाव” जैसी नेपाली कहानियाँ स्त्री के जीवन में जातीयता, निर्धनता और परंपरा के दबाव को उजागर करती हैं। यह शोध तुलनात्मक साहित्य की पद्धति पर आधारित है, जिसमें कहानी के कथ्य, पात्र, भाषा, शिल्प और संवेदना के स्तर पर अध्ययन किया गया है।
| 12 |
Author(s):
तन्मय सेन.
Country:
Research Area:
समाजशास्त्र
Page No:
88-97 |
प्रतीकात्मक से लोकात्मक: जयनगर की मिट्टी की प्रतिमाओं में देवताओं का रूपांतरण
Abstract
यह शोध पत्र इस बात की पड़ताल करता है कि बंगाली संस्कृति में पौराणिक देवताओं - जैसे कृष्ण, बलराम, राधा, दुर्गा और अन्य - को जयनगर माजिलपुर की पारंपरिक मिट्टी की गुड़िया बनाने की प्रथाओं के माध्यम से स्थानीय रूपों में कैसे बदला गया है। ये आकृतियाँ, जो कभी शास्त्रीय प्रतीकात्मकता का हिस्सा थीं, को सरलीकृत, जीवंत और अभिव्यंजक रूपों में फिर से कल्पना की गई है जो बंगाल के ग्रामीण सौंदर्यशास्त्र और सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती हैं। महज खिलौने होने से कहीं आगे, ये गुड़िया स्थानीय अनुष्ठानों और लोक कथाओं में धार्मिक, प्रदर्शनकारी और प्रतीकात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं।
| 13 |
Author(s):
श्री सत्यजीत विश्वास, डॉ. लवनीश शर्मा.
Country:
Research Area:
ललित कला
Page No:
98-106 |
छऊ शिल्प: धार्मिक अनुष्ठान और कलात्मक नवाचार की सहयात्रा
Abstract
छऊ, भारत के पूर्वी क्षेत्रों विशेषतः पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओड़िशा से उत्पन्न एक पारंपरिक भारतीय नृत्य रूप है, जिसमें जीवंत रंगों और बारीकी से निर्मित मुखौटों का प्रयोग कर सांस्कृतिक आख्यानों, पौराणिक कथाओं और स्थानीय लोककथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। यह शोध-पत्र छऊ मुखौटों में प्रयुक्त रंगों और डिजाइनों के प्रतीकात्मक महत्व का अध्ययन करता है, और यह दर्शाता है कि किस प्रकार ये मुखौटे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवाहन में सहायक होते हैं। नृवंशविज्ञानात्मक (ethnographic) और व्याख्यात्मक (interpretative) दृष्टिकोण से किया गया यह अध्ययन यह उजागर करता है कि छऊ मुखौटे केवल सौंदर्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि वे सामुदायिक पहचान, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और लोककथात्मक संवाद के सशक्त माध्यम भी हैं।
| 14 |
Author(s):
श्री लेखराज मांडलेय, डा. प्रमोद कुमार कुर्रे.
Country:
Research Area:
इतिहास
Page No:
107-113 |
छत्तीगढ़ के शैल चित्रकला – रायगढ़ एवं सारंगढ़ जिले के विशेष संदर्भ में
Abstract
संसार के मानव जाति की हर सभ्यता वक्त की रेत पर अपने निशान छोड़ जाती है, ऐसे ही शैलचित्रों की अनोखी दुर्लभ श्रृंखला छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायगढ़ और सारंगढ़ जिले की पहाडिय़ों में बिखरी हुई है, जो सदियां बीतने पर भी धूमिल नहीं हुई है और प्रागैतिहासिक काल से मानव विकास क्रम की कहानियां बयाँ कर रही हैं। रायगढ़ और सारंगढ़ जिले में हजारों वर्ष पुराने पाषाणकालीन समृद्धशाली शैलचित्रों का खजाना है, जो न केवल देश एवं प्रदेश में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसी दुर्लभ पुरासंपदा हमारी प्राचीन सभ्यता के जीवंत अमूल्य अवशेष है। रायगढ़ जिले में आदिम मानवों द्वारा निर्मित शैल चित्र निम्न स्थलों से मिले है - सिंघनपुर, कबरा पहाड़, ओंगना, नवागढ़ पहाड़ी, करमागढ़, बसनाझर, भैंसगढ़ी, खैरपुर, बेनिपाट, ऐसे ही नव निर्मित जिला सारंगढ़ के जैसे अनेक स्थानों में जैसे -सिरौलीडोंगरी ,गाताडीह, बैनीपाट, और बह्मनदेई के शैलाश्रय में शैलचित्र उकेरे गए है, जिनमें पशु-पक्षी, आखेट के दृश्य, परम्परा, जीवनशैली,शिकारों के ये चित्र इनके जीवन के प्रतिबिम्ब थे। इन चित्रों के साथ अनेक सांकेतिक चिन्ह. जैसे -हाथ के पंजों के चिन्ह , गोल या चौकोर अन्य चिन्ह आदि, स्पष्ट है कि विशेष अर्थो लिए प्रयुक्त होते रहे होगे। पर्व एवं त्यौहार का चित्रांकन दीवारों पर किया गया है। ऐसे रॉक पेंटिंग विश्व के अन्य देशों फ्रांस, स्पेन, आस्ट्रेलिया एवं मेक्सिको में भी पाये गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में आदिम मानव इन सघन एवं दुर्गम पहाडिय़ों में गुफाओं एवं कंदराओं में निवास करते थे और यहां सभ्यता का विकास होता गया। आदिम कुशल चित्रकारों द्वारा बनाये इन शैलचित्रों में उनकी जीवनशैली एवं परिवेश की अनुगूंज सुनाई देती है, जिसकी भावनात्मक अभिव्यक्ति इन रेखाचित्रों के रूप में उभरकर सामने आती है। आदिमानव रंगों के प्रयोग से अनभिज्ञ नहीं थे। यह शैलचित्र हमारे पुरखों द्वारा दिया गया बहुमूल्य उपहार है।
| 15 |
Author(s):
भरत कुमार.
Country:
Research Area:
राजनीति विज्ञान
Page No:
114-125 |
राजस्थान के सिरोही जिले में अनुसूचित जनजाति का पंचायतीराज चुनाव 2015 ओर 2020 का तुलनात्मक अध्ययन
Abstract
सारांश
यह अध्ययन सिरोही जिले में पंचायतीराज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों की स्थिति का विश्लेषण करता है, जिसमें वर्ष 2015 और 2020 के बीच की तुलना प्रस्तुत की गई है । प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पंच और सरपंच जैसे जमीनी स्तर के पदों पर महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, जिससे सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सफलता झलकती है । वहीं, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य जैसे मध्य ओर शीर्ष स्तर के पदों पर महिलाओं की भागीदारी में गिरावट दर्ज की गई है, जो चिंता का विषय है । इस अध्ययन में सामने आया है कि कुल प्रतिनिधित्व में लगभग 4.7% की वृद्धि हुई है, किंतु नेतृत्वात्मक पदो पर महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है । यह अध्ययन संबंधित नितियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का का आकलन करने में सहायक हो सकता है तथा भविष्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं स्थानीय शासन में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने हेतु सशक्त बनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है ।
मुख्य शब्द: पंचायतीराज, अनुसूचित जनजाति, सिरोही, राजस्थान, राजनीतिक सहभागिता, जनजातीय सशक्तिकरण
| 16 |
Author(s):
राजीव कुमार झा.
Country:
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
126-131 |
नई कहानी आंदोलन और शैलेश मटियानी की कहानियाँ
Abstract
हिन्दी साहित्य में नई कहानी आंदोलन ने आधुनिकता, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रखकर कहानी लेखन में नए आयाम स्थापित किए। इस आंदोलन के प्रमुख कथाकारों में शैलेश मटियानी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी कहानियाँ सामाजिक हाशिये पर जी रहे लोगों के जीवन, उनकी पीड़ा, संघर्ष और संवेदनाओं को गहरी संवेदनशीलता के साथ उद्घाटित करती हैं। यह शोध आलेख नई कहानी आंदोलन के सैद्धांतिक आधार, इसकी विशेषताओं और शैलेश मटियानी की कहानियों के योगदान का विश्लेषण करता है। शैलेश मटियानी की कहानियों में सामाजिक यथार्थ, निम्न और निम्न-मध्यम वर्ग के चित्रण, आंचलिकता और मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही, उनके साहित्यिक योगदान को समकालीन और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया गया है। यह आलेख शैलेश मटियानी की कहानियों को नई कहानी आंदोलन के संदर्भ में विश्लेषित करते हुए उनके साहित्य की प्रासंगिकता और प्रभाव को रेखांकित करता है।
| 17 |
Author(s):
श्री अभिषेक भट्टाचार्य, डॉ. लवनीश शर्मा.
Country:
Research Area:
ललित कला
Page No:
132-141 |
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दृश्य कला में प्रयोग: भारत में रचनात्मकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का रूपांतरण
Abstract
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) कई रचनात्मक क्षेत्रों में क्रांति ला रही है, जिनमें दृश्य कला भी शामिल है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल कलात्मक सृजन को ही नहीं बदल रही है, बल्कि तकनीक, रचनात्मकता और सांस्कृतिक पहचान के बीच के संबंधों को भी नए सिरे से परिभाषित कर रही है। यह शोध-पत्र भारत में दृश्य कला पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बहुआयामी प्रभावों की पड़ताल करता है, जिसमें समकालीन रचनात्मकता, पारंपरिक कलात्मक अभ्यास, और सांस्कृतिक आख्यानों पर इसका प्रभाव शामिल है। यह अध्ययन अंतःविषय दृष्टिकोण से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कला निर्माण, प्रदर्शन, और व्याख्या में एकीकरण को विश्लेषित करता है, साथ ही इससे जुड़ी नैतिक चिंताओं और भविष्य की संभावनाओं को भी सामने लाता है।
| 18 |
Author(s):
कु. आशा मद्धेशिया, डॉ. पूनम सिंह.
Country:
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
142-146 |
एकभाषी से बहुभाषी समाज की यात्रा : प्रवासी भारतीयों की भूमिका
Abstract
प्रवासी साहित्य एवं भाषा के संदर्भ में सामाजिक-भाषाविदों ने बताया है कि समय परिवर्तनशील होने के कारण भाषा में अनिवार्य रूप से परिवर्तन होंगे। दूसरी तरफ, समकालीन समूदायों के द्वारा प्रत्यक्ष शिक्षण के साथ- साथ इंटरनेट के माध्यम से अभिनव शिक्षण कार्यक्रमों को अपनाकर पैतृक भाषा के उपयोग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।
एकभाषी से बहुभाषी समाज की यात्रा में बॉलीवुड की वैश्विक पहुँच भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक भाषा के रूप में हिंदी से परिचित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
| 19 |
Author(s):
मनोज कुमार झा.
Country:
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
147-158 |
भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्स : वेदांग
Abstract
भारतीय ज्ञान परंपरा की सरणियाँ बहुविध पथों का अवलंबन करती हुई अनादिकाल से प्रवाहित होती आ रही हैं। वेद इस परंपरा के गोमुख हैं। वेदों में भारतीय ज्ञान संपुट रूप में विद्यमान है। यह ज्ञान हजारों वर्षों की कालावधि में संकलित और व्यवस्थित किया गया। श्रीअरविंद ने वेद रहस्य (द सीक्रेट्स ऑफ द वेदाज़) में वैदिक संहिता को भारतवर्ष के धर्म, सभ्यता और आध्यात्मज्ञान का सनातन स्रोत कहा है। वे वेदों को रहस्यमय साहित्य मानते हैं तथा कहते हैं कि वेद, उनकी भाषा, कथन शैली, विचारधारा आदि किसी अन्य युग की सृष्टि हैं, अन्य प्रकार के मनुष्यों की बुद्धि की उपज हैं। एक ओर तो वे अति सरल हैं, मानो निर्मल वेगवती नदी के प्रवाह हों, दूसरी ओर यह विचार-प्रणाली इतनी जटिल लगती है, इसका भाषिक अर्थ इतना गूढ़ है कि मूल विचार तथा पंक्ति के सामान्य अर्थ को समझने में प्राचीन काल से तर्क-वितर्क होता आ रहा है।
| 20 |
Author(s):
डॉ० अलका कल्याण.
Country:
Research Area:
सामाजिक अध्ययन
Page No:
159-168 |
आदिवासी उत्थान में डॉ० आंबेडकर का योगदान
Abstract
प्रस्तुत शोध पत्र में आदिवासी समुदाय के विकास तथा उत्थान में डॉ० बी० आर० आंबेडकर के योगदान को प्रकाशित किया गया है चूँकि डॉ० आंबेडकर को केवल एक दलित नेता के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। जबकि उन्होंने महिला, बाल तथा आदिवासी उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में दलितों के नेता के रूप में डॉ० आंबेडकर तो आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में जयपाल सिंह मुंडा खड़े थे। शोध पत्र में इन दोनों नेताओं के दलित तथा आदिवासी उत्थान के लिए लिए गए फैसले तथा आपसी संवाद को चित्रित कर तत्कालीन परिस्थितियों को दिखाया गया है। इसके साथ साथ भिन्न-भिन्न काल खंड में आदिवासियों को जिन नामों से पुकारा गया उसका विवरण भी उपलब्ध है। संविधान में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखने और संविधान में आदिवासियों के अधिकारों का विवरण शोध प्रत्र में प्रस्तुत है।
| 21 |
Author(s):
ड. विभूतिभूषण महापात्रः.
Country:
Research Area:
संस्कृत
Page No:
169-173 |
ऋग्वेदीयब्रह्मणसाहित्ये सामाजिकवर्णव्यवस्था
Abstract
अस्य शोधपत्रस्य विषयः प्राचीनभारतीयसमाजे वर्णव्यवस्थायाः स्वरूपं विशेषतः ऋग्वेदीयब्रह्मणग्रन्थेषु ब्राह्मणवर्णस्य स्थानम् इत्यस्य विश्लेषणम् अस्ति। वर्णाश्रमव्यवस्था भारतीयसमाजस्य मूलसंरचना आसीत्, या गुण-कर्म-स्वभावाधारेण संस्थिता आसीत्। प्रारम्भे वर्णानां कठोरभेदः नासीत्, किन्तु कालान्तरं तस्य वंशानुगतस्वरूपं जातम्। पुरुषसूक्ते ब्राह्मणस्य उत्पत्तिः मुखात् इति दर्श्यते, येन तस्य बुद्धि, धर्म, त्याग, निष्ठा च मुख्यगुणाः इत्यपि सूच्यन्ते। ब्राह्मणस्य कर्त्तव्यानि—अध्यापनम्, यज्ञानुष्ठानम्, राजोपदेशः, धर्मरक्षणं च। राजनीतिकजीवने ब्राह्मणः राज्ञः प्रमुखः परामर्शदाता आसीत्। सामाजिकजीवने तस्य प्रतिष्ठा मुखवदस्ति, यः यज्ञेन देवतानां सम्पर्कसेतुं साधयति। यद्यपि प्रारम्भे वर्णं गुणकर्माधारेण निर्धारितम्, कालान्तरे सः जात्याधारितः अभवत्। एषा अध्ययनम् ब्राह्मणवर्णस्य महत्त्वं, कर्त्तव्यपरता, तथा समाजे तस्य धार्मिकबौद्धिकप्रभावं प्रकाशयति।
| 22 |
Author(s):
चंचल साह.
Country:
Research Area:
हिन्दी साहित्य
Page No:
174-183 |
नागार्जुन के काव्य में राजनीतिक व्यंग्य
Abstract
आधुनिक साहित्य में शुरुआत से ही अपनी बात कहने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया जाता है । जब भी किसी व्यक्ति, किसी विषय, धर्म, राजनीति आदि पर कटाक्ष करना हो, व्यंग्य ही एकमात्र विकल्प होता है । आधुनिक साहित्य के निर्माता भारतेंदु ने अपने तात्कालिक समय की राजनीति, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक विषमताओं पर कटाक्ष करने के लिए व्यंग्य को ही सहारा बनाया । इसी तरह भारतेंदु युग से लेकर छायावादी युग तक के लगभग सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में व्यंग्यात्मकता को प्रधानता दी है । हिंदी साहित्य का प्रगतिवादी युग विषमताओं का ही युग रहा है। नागार्जुन इस युग के प्रमुख कवि रहे हैं । उनके रचनाकाल 1935 से लेकर उनके मृत्युपर्यंत तक राजनीति में अनगिनत बदलाव हुए । देश को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई पर आम जनता अभी भी अपने ही देश में, अपने ही देश के कुछ नामचीन लोगों के हाथों की कठपुतली थी । देश की स्वतंत्रता पश्चात् भी उनकी जरुरतें, देश के शासकों से उनकी उम्मीदें जब की तस थी । सरकारें बदल रही थी, पर अब भी आमजन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा था । केंद्रीय सत्ता अपने मनमानी करने से बाज़ नहीं आ रहे थे । नागार्जुन राजनीति के इस बदलते परिवेश को महसूस कर रहे थे । नागार्जुन ने राजनीति के इस बदलते परिवेश और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अपनी रचनाओं में व्यंग्य को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया । उन्होंने अपने तीखे व्यंग्यात्मक बाणों से किसी को नहीं बख्शा । सामान्य व्यक्ति के साथ नेतागण, भारत के निर्माणकर्ता, सत्ताधारी वर्ग सभी उनके दृष्टि में थे । उन्होंने अपनी कविताओं में इन सारे वर्गों पर व्यंग्य के माध्यम से तंज कसा । वे एक सशक्त व्यंग्यकार थे ।